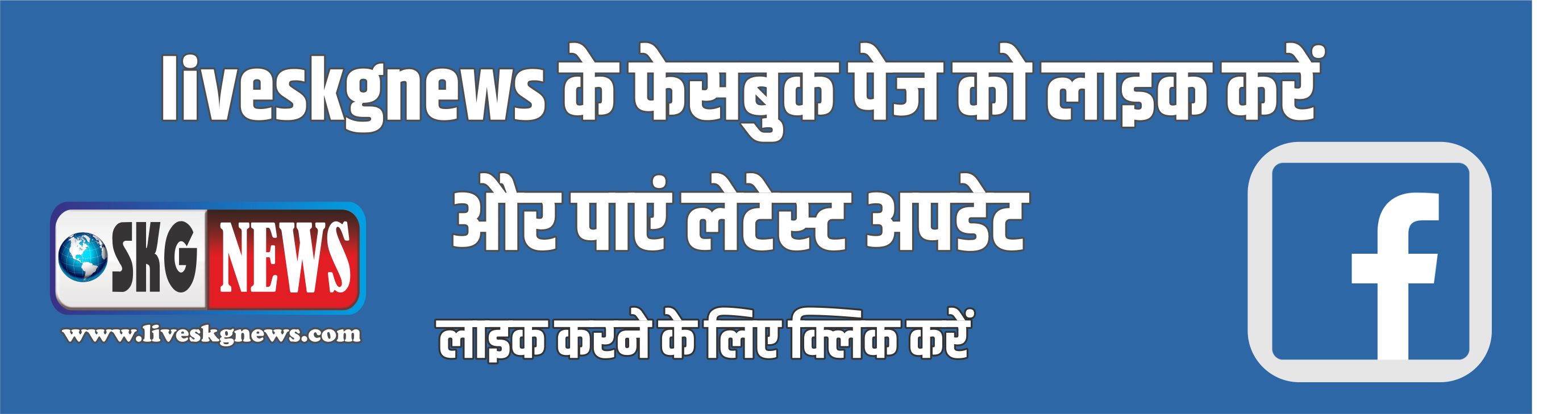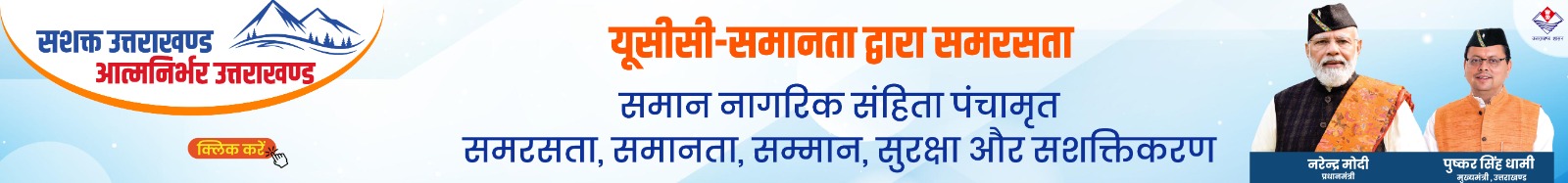नई दिल्ली : मानसून शब्द पूरे भारत में खुशी और गर्व का संचार करता है। यह नवाचार, नवीनीकरण और राष्ट्र के आर्थिक इंजन को तत्काल गति प्रदान करने का प्रतीक है। भारत की भौगोलिक स्थिति, प्रचुर वर्षा के साथ मिलकर, इसकी नदियों को पुनर्जीवित करती है और देशभर में जल संसाधनों का विस्तार करती है। यह प्रगति के मौसम का प्रतीक है और स्वतंत्रता दिवस समारोहों के साथ मिला दिए जाने पर देशभक्ति की एक अनूठी भावना का संचार करता है। लाल किले की प्राचीर से, प्रधानमंत्री के संबोधन ने एक बार फिर आकांक्षी नागरिकों के लिए एक ऐसा खाका पेश किया जो एक विकसित भारत के निर्माण के व्यापक लक्ष्य को साकार करने का मार्ग प्रशस्त करता है।
संसद के इस विशेष मानसून सत्र की शुरुआत में, प्रधानमंत्री ने इसे भारत का गौरवशाली सत्र बताया था। भारतीय सैनिकों का शौर्य, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के कारखानों पर निर्णायक प्रहार और सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) का स्थगन—ये सब भारत की दृढ़ इच्छाशक्ति के सबूत हैं और राष्ट्रीय मानस पर एक अमिट छाप छोड़ते हैं। फिर भी, सभी मुद्दों पर खुलकर चर्चा के लिए सरकार के राजी होने के बावजूद, विपक्ष ने बाधा डालने का रास्ता चुना और व्यापक जनहित की कीमत पर विचार-विमर्श को राजनीतिक नौटंकी में सीमित कर दिया।
देश अरसे से स्वार्थ को राष्ट्रीय हित से ऊपर रखने की कांग्रेस की पुरानी आदत का बोझ ढोता चला आ रहा है। विभाजन की दुखद विभीषिका से लेकर नेहरूवादी कूटनीति की महंगी पड़ने वाली विफलताओं तक, इतिहास गवाह है कि कैसे इन फैसलों ने भारत की मूल अवधारणा को ही कमजोर कर दिया। सिंधु जल संधि (1960) पर बारीकी से गौर करने पर, जनता और देश के विकास की कीमत पर तुष्टिकरण व अति-उदारता की एक ऐसी कहानी सामने आती है, जिसने राष्ट्रीय विकास की संभावनाओं को निरंतर बाधित किया। यह घोर विडंबनापूर्ण है कि भारत के विकास से जुड़े हितों का त्याग एक ऐसे राजनीतिक आकलन से प्रेरित थे जिसने अपने नागरिकों के कल्याण से ऊपर पाकिस्तान के हितों को तरजीह दी।
मूल रूप से, विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुई सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी), सिंधु नदी प्रणाली के जल का आवंटन पाकिस्तान के पक्ष में (80:20) करती है। सिंधु नदी प्रणाली का उद्गम मुख्य रूप से भारत में है। इस संधि के तहत भारत को पश्चिमी में बहने वाली सिंधु, चिनाब और झेलम जैसी महत्वपूर्ण नदियों पर नियंत्रण छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा, जिससे वैसे व्यापक जल संसाधन छिन गए जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के विशाल शुष्क एवं सूखाग्रस्त इलाकों का कायाकल्प कर सकते थे। यदि राष्ट्रीय हितों की रक्षा की जाती, तो सुव्यवस्थित जल अवसंरचना इस इलाके के संपूर्ण विकास की तस्वीर को बेहतर बना सकती थी।
हालांकि, इस महत्वपूर्ण त्याग से व्यापक कूटनीतिक लाभ मिलने की उम्मीदें भ्रामक साबित हुईं। इस संधि के प्रक्रियात्मक संचालन ने चिंताओं को और बढ़ा दिया। इस संधि पर 19 सितंबर 1960 को हस्ताक्षर किए गए थे। लेकिन इसे दो महीने बाद, नवंबर में, संसद के समक्ष रखा गया और वह भी मात्र दो घंटे की औपचारिक चर्चा के लिए। जैसे ही इस संधि से जुड़े तथ्य सामने आए, इसके विभिन्न पहलुओं की पड़ताल के बाद प्रमुख समाचार पत्रों में छपी प्रतिकूल टिप्पणियां सुर्खियों में छायी रहीं। इतने महत्वपूर्ण समझौते के प्रति संसदीय स्तर पर बरते गए इस जल्दबाजी भरे व्यवहार ने लोकतांत्रिक निगरानी, पारदर्शिता और तत्कालीन नेतृत्व की दुर्भावनापूर्ण मंशा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए।
इस सीमित संसदीय पड़ताल के बावजूद, सिंधु जल संधि को भारतीय संसद में भारी विरोध का सामना करना पड़ा। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो उस समय एक युवा सांसद थे, ने चेताते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री नेहरू का यह तर्क बुनियादी रूप से त्रुटिपूर्ण है कि पाकिस्तान की अनुचित मांगों के आगे झुकने से मित्रता और सद्भावना स्थापित होगी।
संसद में 30 नवंबर 1960 को हुई बहस से पता चलता है कि सभी दलों ने इस संधि की आलोचना की थी। अधिकांश सदस्यों ने सरकार की आलोचना की थी और उस पर पाकिस्तान के सामने झुकने तथा भारतीय हितों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया था। राजस्थान से कांग्रेस सांसद हरीश चंद्र माथुर, अशोक मेहता, ए.सी. गुहा, कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद केटीके तंगमणि, सरदार इकबाल सिंह, बृजराज सिंह ने इस जल कूटनीति को लेकर स्पष्ट रूप से चिंताएं जाहिर की थी और इसके विफल होने से जुड़े नतीजों के बारे में अंदेशा जताया था। कुल मिलाकर, इस संधि को “एकतरफा, न कि लेन-देन पर आधारित” कहा जा सकता है।
इस संदर्भ में, यह विडंबना ही थी कि लोकसभा में अपने उत्तर के दौरान प्रधानमंत्री नेहरू ने माननीय सांसदों की बुद्धिमत्ता पर सवाल उठाए और उन्हें कमतर भी आंका। उन्होंने अपने जवाब में कहा कि संसदों द्वारा की गई आलोचना तथ्य और निहित विचारों से अनजान रहने पर आधारित है। उन्होंने (नेहरू) आगे कहा, “मुझे इस बात का दुख है कि इतने महत्वपूर्ण मामले को… एक ऐसा मामला जो न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य से भी जुड़ा है… इतने हल्के में और इतनी लापरवाही एवं संकीर्ण सोच के साथ लिया जा रहा है।”
इस संधि ने भारत के हितों को कुंद कर दिया और यह पाकिस्तान के लिए एक निर्णायक उपलब्धि साबित हुआ। अयूब खान ने एक सार्वजनिक प्रसारण में स्वीकार किया था कि इस संधि की वैधता और गुण-दोष पाकिस्तान के विरुद्ध थे, लेकिन इस मामले में नेहरू की कूटनीतिक विफलता ने पाकिस्तान को बढ़त दिला दी। 4 सितंबर 1960 को रावलपिंडी में अपने प्रसारण में, अयूब खान ने कहा था, “अब जो समाधान हमें मिला है, वह आदर्श नहीं है… लेकिन यह सबसे अच्छा समाधान है जो हमें इन परिस्थितियों में मिल सकता था, इनमें से कई बिंदु, चाहे उनके गुण-दोष और वैधता कुछ भी हों, हमारे खिलाफ हैं।” ये खुलासे आज भी राष्ट्रीय हित को गौण रखने के पीछे के मकसद पर सवाल खड़े करते हैं।
जैसा कि निरंजन डी. गुलाटी ने अपनी किताब “इंडस वाटर ट्रीटी: एन एक्सरसाइज इन इंटरनेशनल मीडिएशन” में लिखा है, 28 फरवरी 1961 को खुद प्रधानमंत्री नेहरू ने इस निराशा को स्वीकार करते हुए कहा था: “मुझे उम्मीद थी कि यह समझौता अन्य समस्याओं के समाधान का रास्ता खोलेगा, लेकिन हम वहीं खड़े हैं जहां पहले थे।” इस संधि के बाद के घटनाक्रम में आया तीखा अंतर इस समझौते की असमानता को और भी गहराई से रेखांकित करता है। नेहरू की ढिलाई और राष्ट्रीय हित को दरकिनार करने की प्रवृत्ति समय के साथ भारी पड़ती गई। फरवरी 1962 में, ‘वाशिंगटन पोस्ट’ को दिए एक साक्षात्कार में, प्रधानमंत्री नेहरू ने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर को “आगे की दिशा में एक बड़ा कदम और वास्तव में यह समझौता (कश्मीर के) क्षेत्रीय मुद्दों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण…” बताया।
स्पष्ट चेतावनियों के बावजूद, शांति और अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति की चाहत में कांग्रेस नेतृत्व ने भारत की दीर्घकालिक जल सुरक्षा एवं समृद्धि के बजाय कूटनीतिक सुविधावाद को चुना। तुष्टिकरण की यह नीति कई मोर्चों पर राष्ट्रीय प्रगति के लिए हानिकारक साबित हुई। इस संधि से अपेक्षित मनोवैज्ञानिक व भावनात्मक लाभ कभी भी साकार नहीं हुए। इसके उलट, यह युद्धों और निरंतर सीमा-पार तनावों के रूप में दुर्भाग्य लेकर आई। जल-बंटवारे की इस सख्त व्यवस्था ने सूखे से लड़ने, सिंचाई व्यवस्था का विस्तार करने और संवेदनशील इलाकों में कृषि को मजबूत करने हेतु अपने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने की भारत की क्षमता को सीमित कर दिया। सत्ता-लोलुप शासकों ने आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के प्रति कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं की, जिससे भारत कमजोर हो गया। वास्तव में, यह संधि भारत के लिए जल कूटनीति की विफलता और पाकिस्तान के लिए एक राजनीतिक विजय थी।
अब, मोदी सरकार इस ऐतिहासिक भूल को सुधारने की दिशा में एक और निर्णायक एवं साहसिक कदम उठा रही है। भारत ने अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अपने संप्रभु अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) को तब तक के लिए स्थगित कर दिया है जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय और अंतिम रूप से सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन देना छोड़ नहीं देता। प्रधानमंत्री मोदी जी का स्पष्ट आह्वान राष्ट्रीय हितों को कमजोर करने वालों के लिए एक कड़ी चेतावनी है: “आतंकवाद और बातचीत साथ-साथ नहीं चल सकते; पानी और खून साथ-साथ नहीं बह सकते।” यह कदम पिछली नीतियों से अलग हटकर एक साहसिक और ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक है। यह केवल एक कूटनीतिक पुनर्संतुलन भर नहीं है, बल्कि अपने संसाधनों और किसानों के हितों एवं संबंधित हितधारकों की आजीविका के अवसरों की रक्षा करने के भारत के संप्रभु अधिकार का एक दृढ़ रणनीतिक दावा है – जो पाकिस्तान की ओर से आने वाले लगातार सीमा पार खतरों के सामने “राष्ट्र प्रथम” के सिद्धांत को सर्वोपरि रखता है।
सिंधु जल संधि का स्थगन कूटनीति से कहीं आगे जाता है—यह विकासशील भारत@2047 के लक्ष्य को साकार करने के भारत के संकल्प को दर्शाता है। अपने जल संसाधनों पर नियंत्रण फिर से हासिल करके, भारत जलवायु के अनुकूल बुनियादी ढांचे का निर्माण कर सकता है, सिंचाई व्यवस्था को मजबूत कर सकता है और औद्योगिक विकास को बढ़ावा दे सकता है—जोकि एक विकसित राष्ट्र बनने की कुंजी है। यह निर्णय पुराने समझौतों द्वारा थोपी गई सहमतियों का अंत करता है और जल संप्रभुता को प्रगति की बुनियाद के रूप में स्थापित करता है। यह एक ऐसा साहसिक कदम है, जो आत्मनिर्भरता, स्थिरता और समावेशी विकास के मिशन के साथ गहराई से जुड़ा है।
- लेखक : अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संसदीय कार्य राज्यमंत्री, भारत सरकार